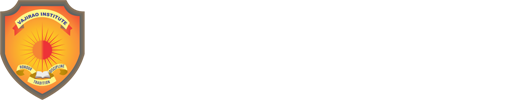संसदीय व्यवस्था से जुड़ी प्राक्कलन समितियाँ:
प्राक्कलन समितियों की प्लेटिनम जयंती:
- 23 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई के विधान भवन में संसदीय प्राक्कलन समितियों की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रमुख राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने में प्राक्कलन समितियों की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसने 1950 से अब तक 1,000 से अधिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। उन्होंने संस्थागत तालमेल, वित्तीय जवाबदेही और प्रौद्योगिकी-संचालित शासन की आवश्यकता पर जोर दिया।
- इसके अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय लोकतंत्र के आवश्यक स्तंभों के रूप में इन समितियों की भूमिका को मजबूत करने के लिए सहयोग और जिम्मेदारी का आह्वान किया।
संसदीय समितियाँ क्या होती हैं?
- भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1921 में मोंटफोर्ड सुधारों के तहत लोक लेखा समिति (PAC) के गठन के साथ हुई थी।
- यद्यपि भारत का संविधान इन समितियों की संरचना, कार्यकाल या कामकाज के बारे में विवरण निर्दिष्ट नहीं करता है, तथापि उनका अधिकार निम्नलिखित से आता है:
- अनुच्छेद 105 (सांसदों के विशेषाधिकार),
- अनुच्छेद 118 (संसद की प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने की शक्ति) और
- लोकसभा प्रक्रिया नियम उनके गठन, नियुक्ति और कामकाज का मार्गदर्शन करते हैं।
- समितियों को नियुक्त, निर्वाचित या नामित किया जाता है और वे अध्यक्ष/सभापति के निर्देश के तहत कार्य करती हैं, तदनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं।
- ये समितियाँ निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं:
- मुद्दों की विस्तृत जाँच
- विशेषज्ञ और हितधारक इनपुट
- जटिल मामलों पर क्रॉस-पार्टी सर्वसम्मति
- इस प्रकार, वे संसदीय निगरानी और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारत में संसदीय समितियों के प्रकार:
- संसदीय समितियों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जाता है:
वित्तीय समितियाँ:
- इसमें प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति (PAC) और सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल हैं।
- इन तीनों की स्थापना 1950 में हुई थी।
विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSC):
- 1993 में स्पीकर शिवराज पाटिल के अधीन शुरू की गईं।
- शुरू में 17, अब 24 समितियों तक विस्तारित की गईं।
- प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं (लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10)। बजट प्रस्तावों और सरकारी नीतियों की जाँच करना, विधायी जाँच को बढ़ाना।
अन्य संसदीय स्थायी समितियाँ:
- ये DRSC और वित्तीय समितियों के अलावा स्थायी समितियाँ हैं, जो पूरे वर्ष विशिष्ट विषयों पर कार्य करती हैं।
तदर्थ समितियाँ:
- किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाई जाती हैं।
- अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद भंग हो जाती हैं।
संयुक्त संसदीय समितियाँ (JPC):
- किसी विशेष विषय या विधेयक की विस्तृत जाँच के लिए बनाई जाती हैं।
- इनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। ये समितियाँ विस्तृत विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, संसदीय कार्य में जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करती हैं।
संसद की प्राक्कलन समिति:
- प्राक्कलन समिति एक वित्तीय स्थायी समिति है, जिसमें तीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिन्हें लोकसभा द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।
- किसी मंत्री को समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाएगा, और यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने के पश्चात मंत्री नियुक्त किया जाता है, तो ऐसा सदस्य ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।
- प्राक्कलन समिति का कार्य:
- अनुमानों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप कौन सी मितव्ययिताएं, संगठन में सुधार, दक्षता या प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं;
- प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव;
- यह जांच करना कि क्या धनराशि अनुमानों में निहित नीति की सीमाओं के भीतर अच्छी तरह से रखी गई है; और
- सुझाव देना कि अनुमानों को संसद में किस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- समिति ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में अपने कार्य नहीं करती है जो लोक सभा के प्रक्रिया नियमों या अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक उपक्रम समिति को आवंटित किए गए हों।
नोट : आप खुद को नवीनतम UPSC Current Affairs in Hindi से अपडेट रखने के लिए Vajirao & Reddy Institute के साथ जुडें.
नोट : हम रविवार को छोड़कर दैनिक आधार पर करेंट अफेयर्स अपलोड करते हैं
Read Current Affairs in English ⇒