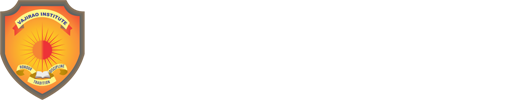1975 का राष्ट्रीय आपातकाल: भारतीय लोकतंत्र के लिए ‘काला अध्याय’ और उससे मिली सीख
मुद्दा क्या है?
- आज से 50 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया। 21 महीनों का यह दौर संविधान, नागरिक अधिकारों के उल्लंघन, प्रेस की अभिव्यक्ति पर रोक और विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां का रहा।
- उल्लेखनीय है कि यह आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक ‘काला अध्याय’ था जो निरंकुश सत्ता के दुरुपयोग, तानाशाही और प्रतिरोध की याद दिलाता है। आपातकाल के बाद हुए घटनाक्रमों ने भारतीय राजनीति एवं संवैधानिक प्रणाली में कई अहम बदलाव भी आए।
आपातकाल का ऐतिहासिक संदर्भ:
- 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद घोषित किया गया, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी दुरुपयोग के कारण पद धारण करने से अयोग्य ठहराया। इस निर्णय ने व्यापक अशांति को जन्म दिया, जिसमें जयप्रकाश नारायण जैसे प्रमुख व्यक्तियों द्वारा नेतृत्व किए गए महत्वपूर्ण विपक्षी आंदोलनों ने भाग लिया। जैसे-जैसे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, श्रीमती गांधी की सरकार पर दबाव बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप ‘आंतरिक अशांति को औचित्य के रूप में उद्धृत करते हुए आपातकाल की विवादास्पद घोषणा हुई।
आपातकाल लागू होने के बाद क्या-क्या हुआ?
- आपातकाल का दौर 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक था, इस दौरान भारत में नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित थीं।
- मौलिक अधिकारों का निलंबन, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता शामिल है।
- विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सामूहिक गिरफ्तारी।
- प्रेस की सेंसरशिप और मीडिया पर नियंत्रण।
- सरकारी नीतियों के हिस्से के रूप में मजबूर नसबंदी और झुग्गी-झोपड़ी का ध्वंस।
- 1977 में कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण चुनावी हार का सामना किया।
नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रभाव:
- आपातकाल के प्रभाव गहन थे। मौलिक अधिकारों, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार शामिल था, को निलंबित कर दिया गया।
- हजारों लोगों को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) के तहत बिना मुकदमे के कैद किया गया, और मीडिया को गंभीर सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। नारायण और जनसंघ के सदस्यों जैसे उच्च-प्रोफाइल विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया।
- जनता ने मजबूर नसबंदियों और झुग्गियों के ध्वंस को देखा, जिसने सरकार के खिलाफ असंतोष को और बढ़ा दिया।
भारत में आपातकाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
- भारत के संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित आपातकालीन प्रावधान तीन अलग-अलग प्रकार की आपात स्थितियों के बारे में बात करते हैं। उल्लेखनीय रूप से, ये प्रावधान जर्मन वेमर संविधान से उधार लिए गए हैं।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 “आपातकाल की घोषणा” से संबंधित है।
- अनुच्छेद 353 “आपातकाल की घोषणा के प्रभाव” के बारे में प्रावधान प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 354 “आपातकाल की घोषणा के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों के आवेदन” के बारे में बात करता है।
- अनुच्छेद 355 “बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने के संघ के कर्तव्य” से संबंधित है।
- अनुच्छेद 356 “राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान” प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 357 “अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग” से संबंधित है।
- आपातकाल लागू होते ही अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 (“स्वतंत्रता का अधिकार”) द्वारा लगाई गई सभी सीमाओं से मुक्त कर देता है।
- अनुच्छेद 359 “आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन” के संबंध में प्रावधान प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान दिए गए हैं।
भारत में कितनी बार आपातकाल लगाया गया है?
- अब तक भारत में तीन बार आपातकाल लगाया जा चुका है:
- पहली बार आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत-चीन युद्ध के आधार पर लगाया गया था।
- दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान युद्ध के आधार पर लगाया गया था।
- तीसरी बार आपातकाल की घोषणा 25 जून, 1975 को “आंतरिक अशांति” के कारण की गई थी।
भारतीय संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों को मान्यता दी गई है?
- संविधान के भाग XVIII में उल्लिखित विभिन्न प्रावधान तीन प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान करते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352-354, 358-359), राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 355-357), वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।
राष्ट्रीय आपातकाल:
- संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर, आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं, यदि भारत या देश के किसी हिस्से की सुरक्षा को “युद्ध या बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह” से खतरा हो।
- नोट: 1975 में, सशस्त्र विद्रोह के बजाय, आपातकाल की घोषणा करने के लिए सरकार के पास “आंतरिक अशांति” का आधार उपलब्ध था। इस प्रकार के आपातकाल को आमतौर पर “राष्ट्रीय आपातकाल” कहा जाता है।
राष्ट्रपति शासन:
- अनुच्छेद 356 (1) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने पर या अन्यथा, संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा-
- राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य तथा राज्यपाल या राज्य के विधानमंडल से भिन्न किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले लेना;
- यह घोषित कर सकेगा कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जा सकेंगी;
- ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो राष्ट्रपति को उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों, जिनके अंतर्गत राज्य में किसी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्णतः या भागतः निलंबित करने के उपबंध भी हैं।
वित्तीय आपातकाल:
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है।
- इसमें कहा गया है, “यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकता है”।
1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान और उसके बाद प्रमुख संवैधानिक निहितार्थ क्या थे?
- 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने के बाद देश में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए क्योंकि आपातकाल की घोषणा ने संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में बदल दिया क्योंकि संघ सरकार को राज्य सरकारों, जो कि निलम्बित तो नहीं हुआ, लेकिन केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ गया, को कोई भी निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हुआ।
- समाचार-पत्रों पर पूर्व-सेंसरशिप लागू कर दी गई। यूएनआई और पीटीआई को समाचार नामक एक राज्य-नियंत्रित एजेंसी में विलय कर दिया गया।
- इसके अतिरिक्त संविधान में भी कुछ ऐसे संशोधन किये
- 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल ने भारत के संविधान के विभिन्न पहलुओं में कई बदलाव लाए गए, जो लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करने वाले थे।
1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विभिन्न संवैधानिक परिवर्तन:
- 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किए गए कुछ प्रमुख संवैधानिक परिवर्तन इस प्रकार थे:
- 38वाँ संविधान संशोधन: न्यायपालिका को आपातकाल की घोषणा और उससे संबंधित अध्यादेशों या कानूनों की समीक्षा करने से रोक दिया गया।
- 39वाँ संविधान संशोधन: प्रमुख अधिकारियों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष) के चुनाव को न्यायिक जाँच से बाहर रखा गया।
- 42वाँ संविधान संशोधन:
- चुनाव विवादों की सुनवाई करने की न्यायपालिका की शक्ति को कम कर दिया गया।
- राज्यों पर केंद्र सरकार के अधिकार को मजबूत किया गया।
- न्यायिक समीक्षा के बिना संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को असीमित शक्ति दी गई।
- निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने वाले कानूनों को अदालती चुनौतियों से मुक्त कर दिया गया।
- निश्चित ही इन संशोधनों ने न्यायिक स्वतंत्रता और संघीय संतुलन को काफी हद तक कमजोर कर दिया, जिससे आपातकाल के दौरान सत्ता केंद्रीकृत हो गई।
प्रतिरोध और परिणाम:
- केंद सरकार के विरोध को दबाने के प्रयासों के बावजूद, प्रतिरोध आंदोलन ने गति पकड़ी, जो जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्चे और भूमिगत प्रकाशनों का उपयोग कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय निंदा भी बढ़ी, जिसने आपातकाल को लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन के रूप में देखने की धारणा को बढ़ावा दिया।
- अंततः, इंदिरा गांधी ने 21 मार्च 1977 को आपातकाल को समाप्त कर दिया, जिसके बाद एक आम चुनाव हुआ जिसमें उनकी पार्टी को महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ा।
44वाँ संविधान संशोधन:
- उल्लेखनीय है कि जनता पार्टी सरकार ने 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए कई संवैधानिक परिवर्तनों को उलट दिया। इसने आपातकाल के प्रावधान को खत्म नहीं किया, लेकिन भविष्य में इसे लागू करना बेहद मुश्किल बना दिया।
- इसने आपातकाल की घोषणा की न्यायिक समीक्षा को फिर से संभव बना दिया और अनिवार्य कर दिया कि आपातकाल की हर घोषणा को घोषणा के एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। जब तक इसे दोनों सदनों अलग-अलग द्वारा विशेष बहुमत से मंजूरी नहीं मिल जाती – सदन की कुल ताकत का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई – उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी।
- 44वें संविधान संशोधन ने आपातकाल लगाने के आधार के रूप में “आंतरिक अशांति” को हटा दिया, और ‘युद्ध’ और ‘बाह्य आक्रमण’ के अलावा अब ‘सशस्त्र विद्रोह’ ही आपातकाल लगाने का आधार होगा।
- हालांकि, 44वें संविधान संशोधन ने 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में डाले गए ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्दों को अछूता छोड़ दिया, जिसको लेकर आज भी अनेक लोग उनकी आलोचना करते हैं और इनको भी संशोधन की वकालत करते हैं।
शाह आयोग और उसकी रिपोर्ट:
- आपातकाल लागू करने और उसके प्रतिकूल प्रभावों पर रिपोर्ट देने के लिए जनता सरकार द्वारा गठित शाह आयोग ने एक निंदनीय रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पाया गया कि यह निर्णय एकतरफा था और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था।
1975 के राष्ट्रीय आपातकाल से संवैधानिक सबक क्या रहे हैं?
- 1975 का आपातकाल लोकतंत्र के लिए खतरों की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है जब सत्ता अनियंत्रित होती है। यह जवाबदेही, कानून के शासन और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है।
- ऐसे में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है:
- एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सशक्त न्यायपालिका
- एक स्वतंत्र और सतर्क प्रेस
- एक मजबूत राजनीतिक विपक्ष और,
- एक सक्रिय और संलग्न नागरिक समाज
- उपर्युक्त संस्थाएँ पिछली गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं।
नोट : आप खुद को नवीनतम UPSC Current Affairs in Hindi से अपडेट रखने के लिए Vajirao & Reddy Institute के साथ जुडें.
नोट : हम रविवार को छोड़कर दैनिक आधार पर करेंट अफेयर्स अपलोड करते हैं
Read Current Affairs in English ⇒