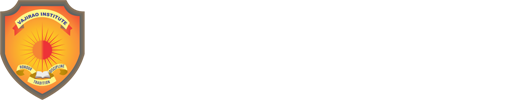जलवायु सक्षम विकास केंद्र के रूप में शहरी भारत को सशक्त बनाने की आवश्यकता:
परिचय:
- भारत का शहरी परिदृश्य तेज़ी से विस्तार कर रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में गंभीर चुनौतियाँ सामने आ रही हैं।
- केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के सहयोग से विश्व बैंक की एक रिपोर्ट (“भारत में लचीले और समृद्ध शहरों की ओर”), शहरी जलवायु लचीलेपन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
- यह रिपोर्ट शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के लिए अधिक स्वायत्तता की वकालत करती है और 2050 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता का सुझाव देती है।
रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:
जलवायु शासन में शहरी स्वायत्तता की आवश्यकता:
- विश्व बैंक भारत के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे ने इस बात पर ज़ोर दिया कि निर्णय लेने की स्वायत्तता वाले शहर जलवायु लचीलेपन में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
- उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन की वकालत की।
- विकेंद्रीकरण से संसाधनों का बेहतर संग्रहण, परिसंपत्ति मुद्रीकरण, राजस्व सृजन और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
शहरी जलवायु जोखिम और आर्थिक लागत:
- शहरी भारत को दो बड़े झटकों का सामना करना पड़ेगा –
- वर्षाकालीन बाढ़ (खराब जल निकासी और अत्यधिक कंक्रीटीकरण के कारण शहरी बाढ़)।
- अत्यधिक गर्मी का तनाव, जो शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव से और भी बदतर हो जाएगा।
- अनुमानित वार्षिक बाढ़-संबंधी नुकसान 2030 तक 5 अरब डॉलर और 2070 तक 30 अरब डॉलर है।
- गर्मी से संबंधित मौतें 2050 तक दोगुनी होकर 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो सकती हैं।
वित्तीय और जनसंख्या अनुमान:
- निवेश आवश्यकताएँ:
- लचीले बुनियादी ढाँचे और सेवाओं के निर्माण के लिए 2050 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।
- अगले 15 वर्षों में 60% उच्च-जोखिम वाले शहरों में बाढ़ से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिए कम से कम 150 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी।
- शहरी विकास पथ:
- 2050 तक शहरी जनसंख्या लगभग दोगुनी होकर 95.1 करोड़ हो जाएगी।
- 2030 तक, शहर भारत में 70% नए रोजगार पैदा करेंगे।
रिपोर्ट की सिफारिशें:
- राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के लिए:
- वित्तपोषण का रोडमैप तैयार करें।
- नगरपालिका क्षमता बढ़ाने के लिए मानक और ढाँचे निर्धारित करें।
- जलवायु-रोधी बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र को शामिल करें।
- शहरों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए:
- स्थानीय स्तर पर जलवायु जोखिमों का मूल्यांकन करें।
- अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी (निजी निवेश सहित) जुटाएँ।
- ऐसी रणनीतियाँ अपनाएं जैसे – ठंडी छतें, पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, शहरी हरियाली, और गर्मी के तनाव को कम करने के लिए काम के घंटों में बदलाव। शहरी नियोजन जो अभेद्य सतहों को कम करता है और तूफानी जल प्रबंधन में सुधार करता है।
भारत में उद्धृत सर्वोत्तम प्रथाएं:
- अहमदाबाद ने एक हीट एक्शन प्लान मॉडल विकसित किया है।
- कोलकाता ने शहर-स्तरीय बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली अपनाई है।
- इंदौर ने एक आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में निवेश किया है।
- चेन्नई ने एक जलवायु कार्य योजना अपनाई है जो गहन जोखिम मूल्यांकन पर आधारित है और अनुकूलन तथा निम्न-कार्बन विकास, दोनों को लक्षित करती है।
नोट : आप खुद को नवीनतम UPSC Current Affairs in Hindi से अपडेट रखने के लिए Vajirao & Reddy Institute के साथ जुडें.
नोट : हम रविवार को छोड़कर दैनिक आधार पर करेंट अफेयर्स अपलोड करते हैं
Read Current Affairs in English ⇒