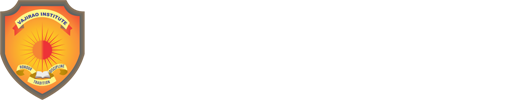भारत के PM2.5 प्रदूषण में एक तिहाई योगदान द्वितीयक प्रदूषकों का है: CREA
चर्चा में क्यों है?
- ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (CREA) हाल ही में जारी एक नए विश्लेषण के अनुसार, द्वितीयक प्रदूषक, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया के बीच वायुमंडलीय प्रतिक्रियाओं से बनने वाले अमोनियम सल्फेट, भारत के सूक्ष्म कण पदार्थ (PM2.5) प्रदूषण का लगभग एक तिहाई हिस्सा हैं।
- अध्ययन में पाया गया कि कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्र, जो देश के सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 60 प्रतिशत से अधिक उत्पन्न करते हैं, इन हानिकारक द्वितीयक कणों के प्राथमिक स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राज्य की सीमाओं के पार वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
भारत में द्वितीयक PM2.5 प्रदूषण:
- 2.5 माइक्रोन से छोटे कण (PM2.5) वायु प्रदूषण के सबसे खतरनाक घटकों में से एक हैं , जो गंभीर श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं।
- उल्लेखनीय है कि परंपरागत रूप से, जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न कालिख और धूल जैसे प्राथमिक प्रदूषकों को PM2.5 के स्तर में मुख्य योगदानकर्ता माना जाता रहा है। हालांकि, नए शोध से भारत की वायु प्रदूषण चुनौती के प्रमुख घटक के रूप में द्वितीयक प्रदूषकों, विशेष रूप से अमोनियम सल्फेट के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक:
- प्राथमिक प्रदूषक सीधे उत्सर्जन स्रोतों जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं, कोयला आधारित बिजली संयंत्र और बायोमास दहन से उत्पन्न होते हैं।
- इसके विपरीत, द्वितीयक प्रदूषक तब बनते हैं जब प्राथमिक प्रदूषक एक दूसरे के साथ या जल वाष्प और सूर्य के प्रकाश जैसे वायुमंडलीय तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं।
- इन प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट जैसे जटिल कण बनते हैं, जो समान या अधिक हानिकारक हो सकते हैं।
CREA अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:
- ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (CREA) के अध्ययन के अनुसार, द्वितीयक प्रदूषक, विशेष रूप से अमोनियम सल्फेट, भारत के PM2.5 द्रव्यमान का 34% तक हिस्सा बनाते हैं।
- भारत सालाना 11.2 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक है और 10.4 मिलियन टन अमोनिया उत्सर्जन के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है। ये बढ़े हुए स्तर सल्फेट, नाइट्रेट और ओजोन यौगिकों सहित व्यापक द्वितीयक प्रदूषक निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाते हैं।
- इस व्यापक उपस्थिति की पहचान उपग्रह-आधारित इमेजरी और वायुमंडलीय मॉडलिंग का उपयोग करके की गई।
सीमा पार प्रकृति से राष्ट्रव्यापी प्रभाव:
- पूरे भारत में अमोनियम सल्फेट की औसत सांद्रता 11.9 μg/m³ पाई गई।
- ये संकेन्द्रण केवल प्रदूषण केन्द्रों के निकटवर्ती शहरों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वायु प्रदूषण की सीमापारीय प्रकृति के कारण ये पूरे देश में फैले हुए हैं।
- द्वितीयक प्रदूषण की सीमा पार प्रकृति वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए विशेष चुनौतियां प्रस्तुत करती है। इस घटना का अर्थ है कि बड़े स्थानीय उत्सर्जन स्रोतों के बिना भी शहरों में द्वितीयक कण परिवहन के कारण PM2.5 का स्तर ऊंचा हो सकता है।
कोयला संयंत्र प्रमुख स्रोत:
- भारत में अमोनियम सल्फेट के पूर्ववर्ती सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन का 60% से अधिक हिस्सा कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा है।
- ये सुविधाएं द्वितीयक PM2.5 निर्माण का प्राथमिक चालक बन जाती हैं।
- कोयला विद्युत संयंत्रों के 10 किलोमीटर के भीतर, अमोनियम सल्फेट की सांद्रता उस सीमा से बाहर के क्षेत्रों (6 μg/m³) की तुलना में 2.5 गुना अधिक (15 μg/m³) थी।
- इन संयंत्रों के निकट, यह PM2.5 प्रदूषण का 36% हिस्सा है, जबकि दूरदराज के क्षेत्रों में भी इसका योगदान 23% है।
- अमोनियम सल्फेट की सबसे अधिक सांद्रता वाले पांच शहरों में पटना 22.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, मुजफ्फरपुर, कोलकाता और हावड़ा 21.7 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर और वाराणसी 21.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर शामिल हैं। सबसे अधिक प्रतिशत योगदान वाले शहरों में कोरबा 43.1 प्रतिशत, भिलाई 42.5 प्रतिशत और अनपरा 42.3 प्रतिशत शामिल हैं।
शमन हेतु रणनीतियाँ:
- द्वितीयक प्रदूषकों के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है:
- उत्सर्जन मानदंडों का सख्त कार्यान्वयन: कोयला बिजली संयंत्रों में एफजीडी स्थापना के प्रवर्तन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। विनियामक रोलबैक सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के लिए प्रतिकूल होगा।
- कृषि और औद्योगिक सुधार: कुशल उर्वरक प्रबंधन से अमोनिया उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, जो द्वितीयक कणों के निर्माण में एक प्रमुख अभिकारक है।
- स्रोत-विशिष्ट कार्रवाई: प्रदूषण न्यूनीकरण प्रयासों को प्रत्यक्ष उत्सर्जन स्रोतों और SO₂ तथा NH₃ जैसी पूर्ववर्ती गैसों दोनों को लक्षित करना चाहिए।
- सीमापार सहयोग: द्वितीयक प्रदूषकों की फैलाव प्रकृति को देखते हुए, प्रभावी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राज्यों के बीच क्षेत्रीय समन्वय आवश्यक है।
- वास्तविक समय निगरानी और अनुसंधान: प्रदूषण गतिशीलता में उभरते पैटर्न की पहचान करने के लिए वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना में निवेश और निरंतर डेटा-आधारित अनुसंधान की आवश्यकता है।
नोट : आप खुद को नवीनतम UPSC Current Affairs in Hindi से अपडेट रखने के लिए Vajirao & Reddy Institute के साथ जुडें.
नोट : हम रविवार को छोड़कर दैनिक आधार पर करेंट अफेयर्स अपलोड करते हैं
Read Current Affairs in English ⇒