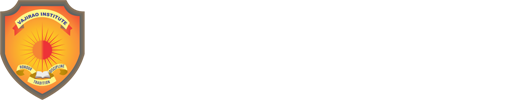भारत में प्रजनन दर में गिरावट के बारे में लिंग भेद लेंस क्या बताता है?
परिचय:
- 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसमें वैश्विक निर्णय लेने में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व और संरचनात्मक बाधाओं को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- भारत के विशेष संदर्भ में यह चिंता ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भी परिलक्षित होती है, जहाँ भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है, जिसका समता स्कोर 64.1% है – जो दक्षिण एशिया में सबसे कम है। कम समग्र रैंकिंग के बावजूद, भारत ने स्वास्थ्य और उत्तरजीविता श्रेणी में सुधार दिखाया है, विशेष रूप से जन्म के समय लिंग अनुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा।
- उल्लेखनीय है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक नीति बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है, जो सरकारों को लिंग असमानताओं को अधिक प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और संबोधित करने में मदद करती है।
भारत में घटती प्रजनन दर और इसके व्यापक प्रभाव:
- UNFPA की 2025 की रिपोर्ट और NFHS-5 (2019-21) के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) गिरकर 2.0 हो गई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। यह गिरावट व्यक्तिगत पसंद से कहीं अधिक को दर्शाती है; यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों द्वारा आकार लेती है, जो सीमित प्रजनन स्वतंत्रता को उजागर करती है।
- 14 देशों (भारत सहित) में किए गए UNFPA -YouGov सर्वेक्षण में पाया गया:
- 20% उत्तरदाताओं को डर है कि वे अपनी इच्छित संख्या में बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे।
- पांच में से एक ने जलवायु परिवर्तन, युद्ध और महामारी को बाधा के रूप में उद्धृत किया।
- भारत में, कम प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं:
- वित्तीय बाधाएँ (38%)
- बेरोज़गारी और नौकरी की असुरक्षा (21%)
- आवास संबंधी समस्याएँ (22%)
- अपर्याप्त चाइल्डकैअर सुविधाएँ (18%)
- प्रजनन-संबंधी स्वास्थ्य सेवा में बाधाएँ (14%)
- दीर्घकालिक बीमारी या खराब स्वास्थ्य (15%)
- ये रुझान वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक में भारत की निम्न रैंकिंग से भी संबंधित हैं, जो दर्शाता है कि प्रजनन क्षमता प्रणालीगत असमानताओं और बाहरी दबावों से कैसे प्रभावित होती है।
- संक्षेप में, भारत में प्रजनन विकल्प संरचनात्मक स्थितियों से गहराई से जुड़े हुए हैं, जो इसे न केवल एक व्यक्तिगत मामला बनाता है, बल्कि व्यापक सामाजिक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब बनाता है।
प्रजनन संबंधी विकल्प के पीछे सामाजिक कारक:
NFHS-5 के अनुसार, पूरे भारत में प्रजनन दर (TFR) में व्यापक अंतर है:
- प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर (2.1): बिहार (2.98), उत्तर प्रदेश (2.35), झारखंड (2.26), मेघालय (2.91), मणिपुर (2.17)
- प्रतिस्थापन स्तर से नीचे: केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे दक्षिणी और पश्चिमी राज्य (1.6-1.9)
- शहरी TFR : 1.6
- ग्रामीण TFR : 2.2
देश में प्रजनन क्षमता के निर्धारक कारक:
- उल्लेखनीय है कि उच्च प्रजनन क्षमता अक्सर कम महिला शिक्षा और एजेंसी से जुड़ी होती है, जबकि कम प्रजनन क्षमता आर्थिक सुरक्षा और वृद्ध आबादी के बारे में चिंता पैदा करती है। हालांकि अक्सर इसे व्यक्तिगत रूप से देखा जाता है, प्रजनन क्षमता के फैसले निम्नलिखित द्वारा आकार लेते हैं:
- राज्य और सामाजिक सहायता प्रणाली (स्वास्थ्य सेवा, मातृत्व लाभ, आदि)
- कार्यस्थल पूर्वाग्रह: वॉयस ऑफ वूमेन स्टडी 2024 से पता चलता है कि महिलाओं को मातृत्व अवकाश जैसी परिवार के अनुकूल नीतियों का उपयोग करने के लिए करियर दंड का सामना करना पड़ता है।
- माता-पिता बनने को आर्थिक और करियर के लिहाज से एक समझौता माना जाता है, खास तौर पर महिलाओं के लिए:
- संस्थागत समर्थन की कमी (जैसे, बच्चों की देखभाल, माता-पिता की छुट्टी, लचीला काम)
- रोजगार और पदोन्नति में लैंगिक पूर्वाग्रह
- इसके साथ-साथ भारत में प्रजनन संबंधी विकल्प केवल व्यक्तिगत नहीं हैं:
- सामाजिक मानदंड (जैसे, बेटे को प्राथमिकता देना) और पारिवारिक दबाव निर्णयों को बहुत प्रभावित करते हैं।
- अनेक विद्वान बताते हैं कि कैसे रिश्तेदारी की संरचना और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह बेटियों का अवमूल्यन करते हैं और महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित करते हैं।
- इसलिए घटती प्रजनन दर को व्यापक सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक संस्थागत वास्तविकताओं के प्रकाश में समझा जाना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर।
भारत में घटती प्रजनन दर पर नीतिगत और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ:
नीतिगत प्रतिक्रिया:
- प्रजनन क्षमता में कमी को दूर करने के लिए अधिकार-आधारित और विश्वास-निर्माण दृष्टिकोण आवश्यक है।
- उल्लेखनीय है कि 2024 में, आंध्र प्रदेश ने अपने पंचायत राज और नगरपालिका अधिनियमों में संशोधन किया, जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों के स्थानीय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हटा दिया गया – इसकी कम TFR (NFHS-5 के अनुसार 1.47 शहरी, 1.78 ग्रामीण) को मान्यता दी गई।
- दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय, माता-पिता बनने को व्यवहार्य बनाने के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
सामाजिक प्रेरक प्रभाव:
- प्रजनन संबंधी निर्णय घरेलू स्थानों में लिंग आधारित भूमिकाओं द्वारा आकार लेते हैं।
- NSO के 2024 के समय उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार:
- 41% महिलाएँ बनाम 21.4% पुरुष देखभाल में भाग लेते हैं।
- महिलाएँ प्रतिदिन 140 मिनट, पुरुष केवल 74 मिनट ऐसे कार्यों पर खर्च करते हैं।
- यह उन मानदंडों को पुष्ट करता है जहाँ अवैतनिक घरेलू काम को महिलाओं की जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है, जो अक्सर बच्चे पैदा करने को हतोत्साहित करता है।
संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता:
- नारीवादी अर्थशास्त्री देवकी जैन ने अपने शोधपत्र “वैल्यूइंग वर्क: टाइम ऐज ए मेजर” (1996) में तर्क दिया है कि अवैतनिक घरेलू श्रम को मान्यता देने और उसका महत्व समझने की आवश्यकता है।
- घरेलू और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों को लैंगिक रूढ़िवादिता से परे जाकर समान रूप से साझा किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष:
- प्रजनन क्षमता में कमी केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि जाति, धर्म, पितृसत्ता और संस्थागत उपेक्षा से प्रभावित एक गहरी सामाजिक चिंता है।
- ऐसे में सूचित और स्वतंत्र प्रजनन विकल्पों का समर्थन करने के लिए नीतिगत सुधार और सामाजिक बदलाव दोनों आवश्यक हैं।
नोट : आप खुद को नवीनतम UPSC Current Affairs in Hindi से अपडेट रखने के लिए Vajirao & Reddy Institute के साथ जुडें.
नोट : हम रविवार को छोड़कर दैनिक आधार पर करेंट अफेयर्स अपलोड करते हैं
Read Current Affairs in English ⇒